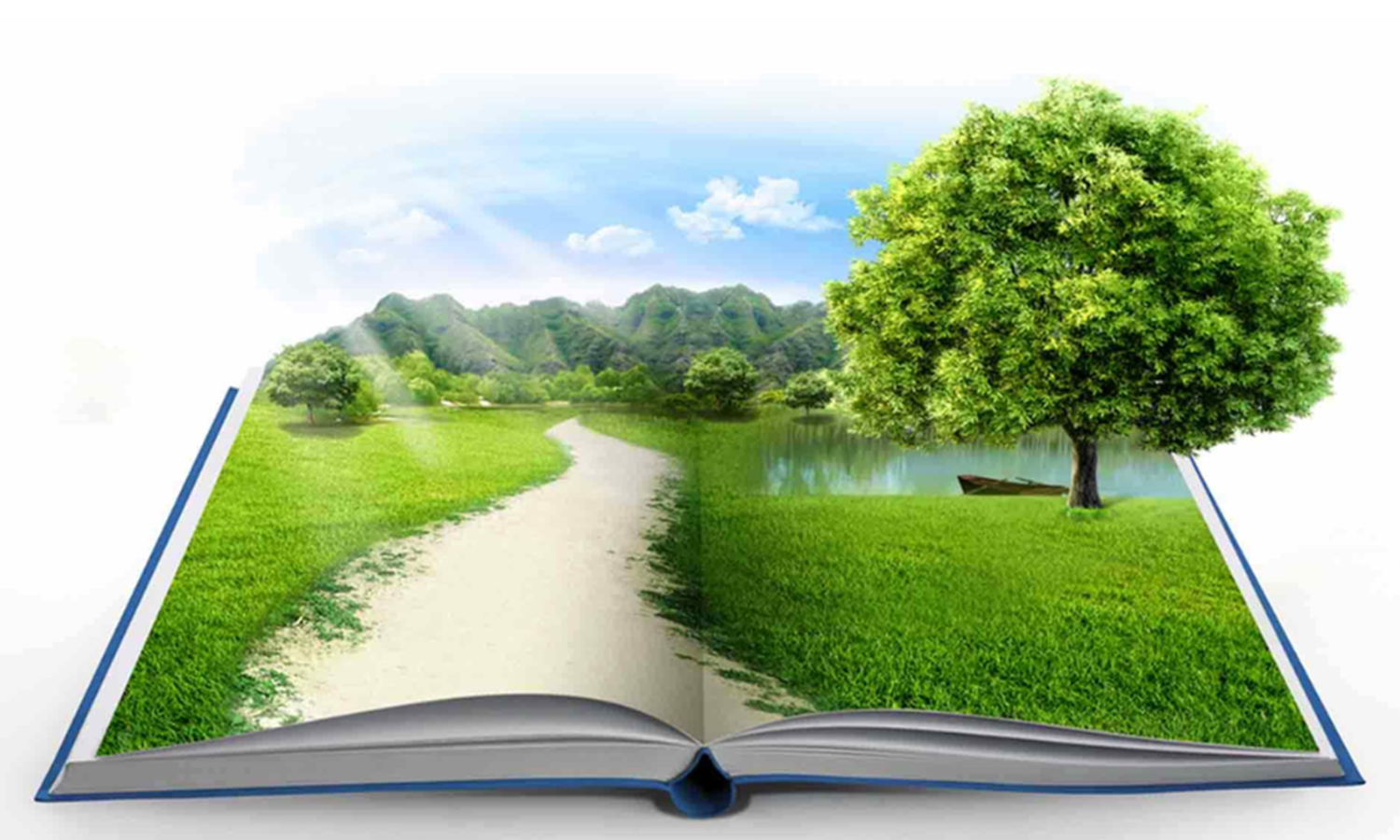पर्यावरण शिक्षा
अजय सहाय
“पर्यावरण शिक्षा: जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध छात्रों की जागरूकता शक्ति” विषय आज के उस वैश्विक यथार्थ को उजागर करता है जहाँ पर्यावरणीय संकट – जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, जैव विविधता क्षरण, वनों की कटाई, जल संकट, और समुद्र तल में वृद्धि – मानव समाज के समक्ष अस्तित्व का संकट बन चुके हैं, और इनसे निपटने के लिए सबसे प्रभावशाली हथियार पर्यावरण शिक्षा ही है, जो छात्रों, युवाओं और अगली पीढ़ी को जागरूकता, वैज्ञानिक समझ और व्यवहारिक भागीदारी के लिए सशक्त बनाती है।
भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ 38 करोड़ छात्र स्कूली और उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत हैं, वहाँ पर्यावरण शिक्षा का दायरा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहकर एक राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ले सकता है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) ने स्पष्ट किया है कि “प्रत्येक छात्र को जलवायु और पर्यावरणीय समझ से लैस करना राष्ट्रीय कर्तव्य है” और इसे विद्यालयी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक लागू किया जाना चाहिए; UNESCO की 2022 की रिपोर्ट “Education for Sustainable Development” के अनुसार यदि वैश्विक स्तर पर हर छात्र को पर्यावरण और जलवायु शिक्षा दी जाए, तो 2050 तक लगभग 60% पर्यावरणीय संकटों को रोकने में मानवीय भूमिका प्रभावी हो सकती है।
वहीं UNEP की 2021 की Emissions Gap Report बताती है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए केवल तकनीकी उपाय पर्याप्त नहीं बल्कि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन ज़रूरी है, जिसमें छात्र, युवा और विद्यालय प्रमुख भूमिका निभाते हैं; भारत में 2003 से पर्यावरण शिक्षा कक्षा 1 से 12 तक अनिवार्य विषय घोषित किया गया, जिसके तहत NCERT ने ‘Our Environment’, ‘Sustainable Development’, ‘Resource Conservation’ जैसे शीर्षकों को पाठ्यक्रम में जोड़ा, 2022 में CBSE ने जलवायु शिक्षा को जीवन कौशल के रूप में ‘Climate Literacy’ मॉड्यूल से जोड़ा, और 2023 में UGC ने सभी विश्वविद्यालयों में “Environmental Studies” विषय को स्नातक स्तर पर क्रेडिट के साथ अनिवार्य कर दिया, यह नीतिगत परिवर्तन लाखों विद्यार्थियों को जलवायु परिवर्तन की वैज्ञानिक समझ, कारण और समाधानों से जोड़ता है।
IPCC की रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि जलवायु संकट का सामना करने के लिए स्थानीय समाधान तभी संभव हैं जब नागरिकों को इसका मूलभूत ज्ञान हो — भारत में 70% छात्र ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और वे जल, भूमि, जंगल, मौसम से प्रत्यक्ष जुड़े होते हैं, ऐसे में यदि इन्हें पर्यावरणीय संकट, कार्बन उत्सर्जन, जल संरक्षण, अक्षय ऊर्जा और जैव विविधता की शिक्षा मिलती है तो वे ग्रामीण स्तर पर जलवायु योद्धा बन सकते हैं।
उदाहरणस्वरूप, बिहार के 38 जिलों में ‘जल जीवन हरियाली क्लब’ और दिल्ली में ‘पर्यावरण ग्रीन ब्रिगेड’ के माध्यम से छात्रों ने स्थानीय जल निकायों, प्लास्टिक उन्मूलन, वृक्षारोपण और वर्षा जल संचयन में सक्रिय भागीदारी की है, साथ ही CBSE के ग्रीन स्कूल कार्यक्रम में 2023 तक 1.2 लाख स्कूलों को ऊर्जा, जल, कचरा और हरित आवरण पर मूल्यांकन में शामिल किया गया; विश्व स्तर पर Fridays for Future, Greta Thunberg, Earth Day Network जैसे आंदोलनों ने यह साबित किया है कि छात्र जलवायु की चेतना के वाहक हो सकते हैं — 2022 में हुए “Earth Hour” अभियान में भारत के 200 शहरों के 45 लाख छात्रों ने एक साथ बिजली बंद कर जलवायु प्रतिबद्धता दिखाई।
वहीं 2023 में “Mission Life” के अंतर्गत 8 करोड़ छात्रों ने पर्यावरणीय संरक्षण की 7 आदतों (7 Life Actions) को अपनाने की प्रतिज्ञा ली, जिसमें प्लास्टिक का त्याग, वर्षा जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, हरियाली संवर्धन शामिल है; वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो छात्रों को जलवायु मॉडल, वायुमंडलीय रसायन, तापमान डेटा, अक्षय ऊर्जा प्रयोगशालाएँ, जल गुणवत्ता परीक्षण और कार्बन फूटप्रिंट मापन जैसे प्रयोगात्मक शिक्षण से जोड़ना आवश्यक है, जैसे IIT गांधीनगर और TERI विश्वविद्यालय ने स्कूली छात्रों के लिए जलवायु विज्ञान आधारित लैब मॉडल विकसित किया है।
जिसमें मौसम रीडिंग, ग्रीनहाउस प्रयोग और जलवायु डेटा का विश्लेषण सिखाया जाता है, वहीं राज्य स्तर पर महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और केरल जैसे राज्यों ने ग्रीन पाठ्यक्रम, छात्र वन, स्कूल सोलराइजेशन, और इको क्लबों को अनिवार्य किया है — जैसे ओडिशा के 22,000 विद्यालयों में “Student Eco Warriors” अभियान चलाया गया जिससे 11 लाख छात्रों ने बायोडायवर्सिटी संरक्षण और कचरा प्रबंधन में भागीदारी की; संयुक्त राष्ट्र SDG 13 (Climate Action) और SDG 4.7 (Sustainability Education) की प्राप्ति में भारत के छात्रों की भागीदारी न केवल राष्ट्रीय दायित्व है बल्कि वैश्विक कर्तव्य भी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन भारत के 75% जिलों को सीधे प्रभावित कर रहा है ।
नीति आयोग की रिपोर्ट 2023 कहती है कि 213 जिले जल संकट और 147 जिले तापीय असमानता से जूझ रहे हैं, इन क्षेत्रों में पर्यावरण शिक्षा छात्रों को न केवल समस्याओं की पहचान सिखाती है बल्कि समाधान हेतु नवाचार, तकनीक और सामाजिक नेतृत्व भी विकसित करती है; जैसे झारखंड, राजस्थान, असम, और उत्तराखंड में छात्रों ने नदियों की सफाई, तालाबों का पुनरुद्धार, प्लास्टिक बैंक, ग्रीन कैंपेन और डिजिटल जल मानचित्रण जैसे प्रयोग किए हैं।
वहीं IIT मद्रास, IISc बैंगलोर और IARI दिल्ली जैसे संस्थानों ने ‘Student Climate Innovation Fund’ की शुरुआत की है जिसमें जलवायु अनुकूल परियोजनाओं को छात्र स्तर पर बढ़ावा मिलता है; ग्रामीण विद्यालयों में भी पर्यावरण जागरूकता लाने हेतु भारत सरकार ने 2022 में “जवाहर नवोदय विद्यालय हरित मिशन” शुरू किया, जिसके अंतर्गत 600+ स्कूलों में वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, सौर ऊर्जा और वृक्षारोपण की परियोजनाएँ चलाई गईं ।
UNICEF और UNEP की 2021 की रिपोर्ट “The Climate Crisis is a Child Rights Crisis” में स्पष्ट कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन सबसे पहले बच्चों को प्रभावित करता है, क्योंकि 90% जलजनित रोग, गर्मी से जुड़ी बीमारियाँ और पोषण संकट 0–19 आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, इसलिए छात्रों को ज्ञान, क्षमता और नेतृत्व प्रदान करना जलवायु न्याय का अभिन्न अंग है ।
यदि भारत के 38 करोड़ छात्रों को जलवायु योद्धा के रूप में प्रशिक्षित किया जाए और इन्हें जलवायु शिक्षा, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी के साथ जोड़ा जाए, तो यह शक्ति देश को 2047 तक जलवायु के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकती है — जहाँ प्रत्येक छात्र वर्ष में 10 पेड़ लगाए, 100 लीटर वर्षा जल संरक्षित करे, 50 किलो प्लास्टिक कम उपयोग करे, और 1 टन कार्बन उत्सर्जन रोके, तो यह प्रयास सामूहिक रूप से 380 करोड़ पेड़, 3.8 अरब लीटर जल, 19 करोड़ किलो प्लास्टिक और 38 करोड़ टन CO₂ के बराबर हो सकता है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से जलवायु संकट के खिलाफ मानव इतिहास का सबसे बड़ा छात्र-आंदोलन होगा।
इसलिए यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं कि “छात्रों की जागरूकता शक्ति” ही आने वाले कल की सबसे बड़ी प्राकृतिक संपदा है — जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाली सशक्त, संवेदनशील और वैज्ञानिक पीढ़ी तैयार कर रही है, और यही भविष्य की जलवायु रक्षा पंक्ति होगी।